दिल्ली-एनसीआर में earthquake के तेज झटके, घरों और ऑफिसों से बाहर निकले लोग
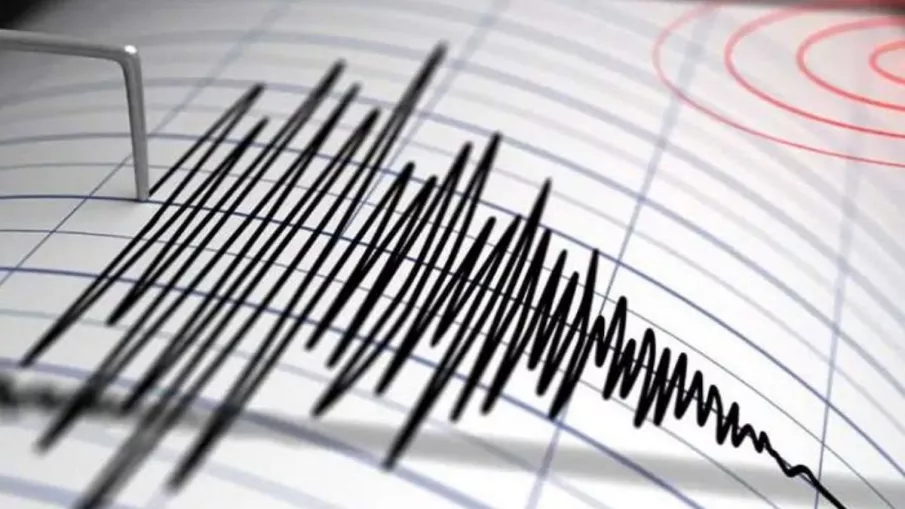
New Delhi: दिल्ली-एनसीआर में भीषण भूकंप (earthquake) के झटके महसूस किए गए हैं। ये झटके गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में बहुत तेज महसूस किए गए। फरीदाबाद में जमीन के 10 किलोमीटर नीचे भूकंप का केंद्र था। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 3.1 मापी गई है। भूकंप (earthquake) करीब 4 बजकर 8 मिनट पर महसूस किया गया। भूकंप के डर से लोग अपने घरों और ऑफिस के बाहर निकल आए। दो हफ्ते में दूसरी बार दिल्ली एनसीआर में भूकंप की वजह से धरती कांपी है।
आज अफगानिस्तान में भी आया था earthquake
आज अफगानिस्तान में भी भूकंप की वजह से धरती कांपी थी। यूरोपीय-भूमध्यसागरीय भूकंप विज्ञान केंद्र (ईएमएससी) ने कहा कि रविवार को पश्चिमी अफगानिस्तान में 6.5 तीव्रता का भूकंप आया। ईएमएससी ने बताया कि भूकंप 10 किमी की गहराई पर था। मिल रही जानकारी के मुताबिक रविवार की सुबह और स्थानीय समयानुसार भूकंप 0336 GMT पर, शहर से 33 किलोमीटर (20 मील) दूर पश्चिमी हेरात प्रांत के एक क्षेत्र में आया, जहां पिछले कई दिनों में आए कई तेज़ झटकों से लगभग 1,000 लोग मारे गए थे। यूएसजीएस ने कहा कि भूकंप आने के ठीक 20 मिनट बाद फिर से 5.5 तीव्रता के झटके महसूस किए गए। भूकंप का एहसास होते ही लोग घरों से बाहर निकल भागे। लोगों के बीच दहशत का माहौल है।
Earthquake in Delhi: दिल्ली एनसीआर में मेहसूस हुए भूकंप के झटके
रिक्टर स्केल पर भूकंप (earthquake) की तीव्रता का अंदाजा कैसे लगा सकते हैं?
-
- 0 से 1.9 सीज्मोग्राफ से मिलती है जानकारी
-
- 2 से 2.9 बहुत कम कंपन पता चलता है
-
- 3 से 3.9 ऐसा लगेगा कि कोई भारी वाहन पास से गुजर गया
-
- 4 से 4.9 घर में रखा सामान अपनी जगह से नीचे गिर सकता है
-
- 5 से 5.9 भारी सामान और फर्नीचर भी हिल सकता है
-
- 6 से 6.9 इमारत का बेस दरक सकता है
-
- 7 से 7.9 इमारतें गिर जाती हैं
-
- 8 से 8.9 सुनामी का खतरा, ज्यादा तबाही
-
- 9 या ज्यादा सबसे भीषण तबाही, धरती का कंपन साफ महसूस होगा
भूकंप (earthquake) क्या है?
साधारण शब्दों में भूकंप का अर्थ है “भूमि का कांपना” अर्थात “पृथ्वी का हिलना”. होम्स के अनुसार, “यदि किसी तालाब के शांत जल में एक पत्थर फेंका जाए तो जल के तल पर सभी दिशाओं में तरंगें फैल जाएगी. इसी प्रकार जब चट्टानों में कोई आकस्मिक हलचल होती है तो उससे कम्पन पैदा होती है.” मैक्सवेल के अनुसार, “भूकंप धरातल के ऊपरी भाग की वह कम्पन विधि है, जो धरातल के ऊपरी तथा निचली चट्टानों के लचीलेपन एवं गुरुत्वाकर्षण की समान स्थिति में कमी आने से प्रारंभ होती है.” सेलिसबरी के अनुसार, “भूकंप वे धरातलीय कम्पन हैं, जो मनुष्य से असंबंधित क्रियाओं के परिणामस्वरूप आते हैं.
भूकंप आने के विभिन्न कारण
1. ज्वालामुखी विस्फोट
जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में हलचल होती है, जिसे भूकंप कहते हैं. कई बार जवालामुखी की ऊपरी कड़ी चट्टानों के अवरोध के कारण लावा बाहर नहीं आ पाता है, जिसके कारण ऊपर की चट्टानों में कम्पन उत्पन्न होता है. इस प्रकार ज्वालामुखी क्षेत्रों में कई बार बिना ज्वालामुखी विस्फोट के भी भूकंप आ जाते हैं.
2. पृथ्वी का सिकुड़ना
पृथ्वी अपने जन्म से लेकर अब तक ठंढी होकर सिकुड़ रही है. पृथ्वी के सिकुड़ने से इसके चट्टानों में अव्यवस्था उत्पन्न होती है, जिससे कम्पन पैदा होता है और भूकंप आता है.
3. बलन तथा भ्रंश
बलन तथा भ्रंश का संबंध क्रमशः संपीड़न तथा तनाव से है, जिससे चट्टानों में हलचल होती है और भूकंप आते हैं. वर्ष 1934 में बिहार का भूकंप, वर्ष 1950 का असम का भूकंप तथा वर्ष 1991 में उत्तर काशी का भूकंप इसी प्रकार के भूकंप थे.
4. भू-सन्तुलन
विद्वानों के अनुसार पृथ्वी का ऊपरी परत “सियाल” हल्का है जो निचले भारी परत “सीमा” पर तैर रहा है. ऊपरी परत पर स्थित हल्की चट्टानों ने ऊपर-नीचे होकर सन्तुलन की व्यवस्था बना ली है. परन्तु जब अपरदन द्वारा उच्च प्रदेशों से शैलचूर्ण अपरदित होकर निम्न प्रदेशों में निक्षेपित होता है तो यह सन्तुलन बिगड़ जाता है. जब चट्टानें इस सन्तुलन को बनाए रखने का प्रयास करती हैं तो उनमें कम्पन उत्पन्न हो जाता है और भूकंप (earthquake) आ जाता है. 4 मार्च, 1949 को लाहौर में इसी प्रकार का भूकंप आया था.
5. प्रत्यास्थ प्रतिक्षेप सिद्धांत (Elastic Rebound Theory)
इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के प्रसिद्ध भू-गर्भवेत्ता डॉ. एस. एफ. रीड ने किया था जिस कारण इसे डॉ. एस. एफ. रीड का सिद्धांत कहा जाता है. इस सिद्धांत के अनुसार भूकंपों की यांत्रिक रचना शैलों के लचीलेपन पर निर्भर करती है. भू-गर्भ की शैलें रबड़ की तरह लचीली होती हैं. जब किसी स्थान पर शैलों पर तनाव बढ़ता है तो वे मुड़ जाती हैं. परन्तु जब तनाव शैलों के लचीलेपन की सीमा से अधिक हो जाता है तो शैलें टूट जाती हैं और दो अलग-अलग खंडों में विभाजित हो जाती हैं. विभाजन के कारण शैल के खंडों के बीच दरार पैदा हो जाती है और दरार के दोनों ओर के चट्टान विपरीत दिशा में खिसक जाते हैं. इस भ्रंश क्रिया से चट्टान का तनाव समाप्त हो जाता है और चट्टान के दोनों खंड अपने स्थान पर आने का प्रयास करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप भूकंप उत्पन्न होता है.
6. प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत (Plate Tectonics Theory)
ज्वालामुखी विस्फोट की भांति भूकंप भी मुख्यतः प्लेटों के किनारों पर ही अधिक आते हैं. कम गहरे केन्द्र वाले भूकंप लगभग सभी प्लेटों के किनारे पर पाए जाते हैं. मध्यम गहराई वाले भूकंपों का केन्द्र लगभग 200 किमी. की गहराई पर होता है. इस तरह के भूकंप महासागरीय खाइयों में मिलते हैं. इन क्षेत्रों में प्लेटें खाई के तल से 300-400 किमी. नीचे चली जाती है. मध्यम गहराई वाले भूकंप तनाव अथवा संपीड़न से पैदा होते हैं, जबकि अधिक गहराई वाले भूकंप केवल संपीड़न से पैदा होते हैं. प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में आने वाले भूकंप का कारण प्लेट विवर्तनिकी ही है.
7. जलीय भार
नदियों पर बाँध बनाकर बड़े-बड़े जलाशयों का निर्माण किया जाता है. जब जलाशयों में जल की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो चट्टानों पर जल का दबाव बढ़ जाता है, जिसके कारण जलाशय के तल में स्थित चट्टानों के आकार में परिवर्तन होने लगता है. जब यह परिवर्तन आकस्मिक होता है तो भूकंप आता है. भारत में इस तरह का भूकंप कोयना बाँध वाले क्षेत्र में 11 दिसम्बर, 1967 को आया था.
8. कृत्रिम भूकंप
कृत्रिम भूकंप (earthquake) मनुष्य के क्रियाकलापों के कारण आते हैं. उदहारण के लिए, बम-विस्फोट, ट्रेन के चलने से तथा कारखानों में भारी मशीनों के चलने से भी पृथ्वी में कम्पन होता रहता है.
9. अन्य कारण
हिमखंडों या शिलाओं के खिसकने तथा गुफाओं की छतों के धंसने या खानों की छतों के गिरने से भी भूकंप आते हैं.
एक वर्ष में कितनी बार भूकंप आते हैं
भूकंपमापी यंत्रों के रिकॉर्ड से पता चलता है कि विश्व में एक वर्ष की अवधि में 8,000 से 10,000 बार भूकंप आते हैं, अर्थात हर एक घंटे बाद विश्व के किसी-न-किसी हिस्से में भूकंप आता है. भूकंपों की वास्तविक संख्या इससे भी अधिक हो सकती है, क्योंकि महासागरों के अधिकांश भाग में भूकंप मापने के केन्द्र अभी तक स्थापित नहीं किए गए हैं और वहां पर आने वाले भूकंपों को प्रायः रिकॉर्ड नहीं किया जाता है. विश्व के अधिकांश भूकंप भू-तल से 50 से 100 किमी. की गहराई पर उत्पन्न होते हैं.
भूकंप का अध्ययन कैसे किया जाता है
भूकंपों का अध्ययन करने वाले विज्ञान को सिस्मोलॉजी (Seismology) और भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को सिस्मोग्राफ (Seismograph) कहा जाता है. भूकंप के कारण जब धरातल पर कम्पन होता है तो उसे प्रधात (Shock) कहते हैं. भूकंप के मूल उद्गम स्थल को केन्द्र (Focus) कहते हैं. केन्द्र के ठीक ऊपर भूतल पर स्थित स्थल को भूकंप का अधिकेन्द्र (Epicentre) कहते हैं. समान भूकंप तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समभूकंप रेखा (Isoseismal line) कहते हैं तथा एक समय पर पहुंचने वाली तरंगों को मिलाने वाली रेखा को सहभूकंप रेखा (Homoseismal line) कहते हैं.





